जीवन का अमृत एवं जीवन का मूलस्रोत मनुष्य के भीतर ही है। मनुष्य के भीतर संस्थित अमृत-कुण्ड ही मनुष्य के अस्तित्व का आधार एवं केन्द्र है। मनुष्य चिन्तन के द्वारा मन्थन करके और ध्यान-प्रक्रिया के द्वारा भीतर और बाहर की चेतनात्मक एकता सिद्ध हो जाती है तथा चेतना का धरातल ऊँचा हो जाने पर मनुष्य भय, चिन्ता, तनाव, कोप, शोक, दुःख आदि से ऊपर उठ जाता है। भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है तथा वह सत्य,प्रेम और शान्ति की उपलब्धि का प्रमुख बाधक है। मृत्यु और विनाश का भय दूर होने पर समस्त भय दूर हो जाता है। मनुष्य अपने भीतर स्थित अमृत-कुण्ड का साक्षात्कार करके मृत्यु एवं विनाश के भय से अर्थात् समस्त भय से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। प्रायः लोग भयवश विश्व की चैतन्य सत्ता के तता अपने भीतर ईश्वरीय शक्ति के आस्तित्व को स्वीकार तो कर लेते हैं किन्तु न उसकी खोज करते हैं और न उसकी प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। ध्यान मनुष्य के अस्तित्व, अमृतत्व एवं आनन्द की अनुभूति के मार्ग की अन्तर्मुखी यात्रा है। मनुष्य को ध्यान द्वारा धैर्यपूर्वक अपने भीतर आनन्द की एवं ऊर्जा के स्रोत की खोज में, उसकी अनुभूति होने तक, अन्तर्यात्रा करते ही रहना चाहिए। मन के विगलित होने पर अथवा मन से परे चले जाने पर मनुष्य को अनन्त आनन्द एवं ऊर्जा की सूक्ष्म अनुभूति होती है तथा अपने दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है।
ध्यान की असंख्य प्रक्रिया हैं तथा सभी महत्त्वपूर्ण हैं। ध्यान से पूर्व अल्प भक्ति-संगीत की भूमिका भी उपयोगी होती है। ध्यान में मन की चंचलता को नियन्त्रित करने के लिए बाह्य आलम्बन का सहारा नहीं लिया जाता। ध्यान द्वारा अभद्र संस्कारों को उखाड़ दिया जाता है और नये संस्कार नहीं बनने दिए जाते। मनुष्य राग-द्वेष से मुक्त हो जाता है तथा अनन्त प्रेम एवं करुणा से परिपूर्ण हो जाता है। मन का निर्मलीकरण ही मन का उदात्तीकरण है। निर्मल एवं उदात्त होने पर बाधक मन साधक हो जाता है तथा मनुष्य खोए हुए आनन्द को प्राप्त कर लेता है।
निश्चय ही तात्कालिक एवं स्थायी शान्ति और स्थिरता प्राप्त करने के लिए ध्यान द्वारा अपने भीतर संस्थित आनन्द के अमृतमय स्रोत से जुड़ना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। मनुष्य ध्यान की साधना द्वारा अपने भीतर प्रच्छन्न दिव्य सत्ता एवं दिव्य चेतना के साथ संयुक्त होकर सहज ही भय और शोक को पार कर लेता है तथा अनन्त आनन्द में संस्थित हो जाता है। ध्यान का सच्चा साधक बिन्दु में सिन्धु के दर्शन एवं पूर्णता की सूक्ष्म अनुभूति करके कृतकृत्य हो जाता है। लक्ष्य के स्पष्ट होने पर, भटकता छोड़कर, संकल्पपूर्वक मार्ग पर चलते रहने और धैर्यपूर्वक आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता होती है। ध्यान ही आध्यात्मिक उपलब्धियों का प्रमुख एवं श्रेष्ठ साधन है।
मनुष्य के मन में विचारों तथा उद्वेगों की क्रिया एवं प्रतिक्रिया मनुष्य के सुख एवं दुःख के लिए उत्तरदायी होती हैं। विचार ही भय क्रोध, शोक, हर्ष आदि उद्वेगों को उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें नियन्त्रण में भी रख सकते हैं। किन्तु जब उद्वेग प्रबल हो जाते हैं, वे विचारों को ही प्रभावित करने लगते हैं और अशान्ति उत्पन्न कर देते हैं। ध्यान का अभ्यास करने पर उद्वेगों की तीव्रता एवं वेग धीरे-धीरे क्षीण होकर लुप्त हो जाते हैं तथा विचार ही उद्वेगों को नियंन्त्रित करने लगते हैं। विचारों द्वारा उद्वेगों का नियंत्रण होना ही आत्म-नियन्त्रण होता है आत्म-नियंत्रण होने से आत्मविश्वास बढ़ जाता है तथा शान्ति का अनुभव सुलभ हो जाता है ध्यान का अभ्यास होने पर मनुष्य को निन्दा और आलोजना की चुभन नहीं होती तथा वह द्वन्द्व से ऊपर उठ जाता है।
मनुष्य का मस्तिष्क स्वाभाविक रूप से निरन्तर सक्रिय रहता है। कभी-कभी विचार सहसा भीड़ उमड़कर ऊपर आते हैं तथा वे न केवल बेतुके होते हैं, बल्कि परस्पर बिलकुल असंबद्ध भी होते हैं। वे प्रतिस्पर्धा में संलग्न धावकों की भाँति झपटपर तेजी से एक-दूसरे से आगे बढते हुए निरर्थक हलचल उत्पन्न कर देते हैं। अनेक विचार प्रारम्भ होते ही विलुप्त हो जाते हैं तथा अनेक विचार स्थिर होकर देर तक सामने बने ही रहते हैं। कभी-कभी विचार बहुत धीरे से आते हैं। प्रायः मनुष्य के लेटने पर, विशेषतः निद्रालुता का अवस्था में, चेतना-स्तर पर स्थित सचेतक के निष्क्रिय हो जाने के कारण अत्यन्त निरर्थक, अधूरे, टूटे-फूटे और असंबद्ध विचार आने लगते हैं तथा कभी-कभी निद्रालुता के सहसा भंग होने पर वे अपनी विचित्रता के कारण मनुष्य को चौका देते हैं। मनुष्य जाग्रत्-अवस्था से स्वप्न-अवस्था में सहसा नहीं जाता तथा अर्द्ध-जाग्रत्-अवस्था में ही स्वप्नों की चित्र-विचित्रता का प्रारम्भ हो जाता है। किन्तु वास्तव में अन्तर्मन की प्रत्येक हलचल प्रच्छन्न रूप से स्वास्थ्यप्रद होती है।
मनुष्य का मन एक समुद्र की भाँति होता है जिसमें ऊपर के स्तर पर लहरों की निरन्तर सक्रियता रहती है तथा नीचे गहरे स्तर पर गम्भीर शांति होती है। ध्यान के अभ्यास से मनुष्य का मन चेतन तथा अचेतन से परे शुद्ध चेतन का गम्भीर दैवी शांति का संस्पर्श करके शांत रहना सीख लेता है तथा भय, हर्ष, शोक, क्रोध आदि उद्वेग उसे विचलित नहीं कर पाते। मनुष्य के लिए मानसिक शांति हेतु समस्याओं से दूर हटकर कुछ अन्य रचनात्मक चिन्तन करना, ध्यान का अभ्यास करना, रुचिप्रद मनोरंजन करना तथा उपयोगी कार्य में व्यस्त होना आवश्यक होता है। ध्यान के द्वारा अमृत के आस्वादन के प्रति उत्कट लालसा उदीप्त हो जाती है ।
The Lodge Goat, Goat Rides, Butts and Goat Hairs, Gathered From the Lodge
Rooms of Every Fraternal Order (Pettibone)
-
The Lodge Goat, Goat Rides, Butts and Goat Hairs, Gathered From the Lodge
Rooms of Every Fraternal Order: More than a Thousand Anecdotes, Incidents
and Ill...
6 months ago
 My Channel
My Channel Cepek Arts
Cepek Arts Cepek Kids
Cepek Kids Cepek Media
Cepek Media Cepek Photography
Cepek Photography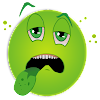 Social Fever
Social Fever
No comments:
Post a Comment