विवेक का जागरण ही मनुष्य को सत्कर्म में प्रवृत्ति करता है तथा कुकर्म से रोकता है। विवेक मनुष्य का आन्तरिक मित्र और सद्गुरु है। किसी अन्य व्यक्ति की सहायता भी निष्फल रहती है यदि मनुष्य का विवेक का प्रकाशदीप प्रज्वलित न हो। अतएव आवश्यकता यह है कि मनुष्य स्वयं ही तथ्यों को समझकर अपने पैरों पर उठ खड़ा हो। धर्म के क्षेत्र में घुसकर भी बुद्धि के द्वार खोले रखने से ही मनुष्य को लाभ हो सकता है तथा बुद्धि के द्वार बन्द कर देने से व्यक्ति का विकास अवरुद्ध हो जाने के कारण घोर हानि हो जाति है। कहीं-कहीं तो संगीत को भी गुनाह बता दिया गया है। मदिरापान, धूम्रपान आदि व्यसनों तथा यौन की भटकनों को भी मनुष्य के भीतर समझदारी और सकंल्प-शक्ति को जगाकर रोका जाना पाप-बय दिखाने की अपेक्षा अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। यद्यपि यौनाचार का नियंत्रण होना निश्चित ही व्यक्ति तथा समाज के हित मे होता है, उस पर पाप के बय द्वारा बरबस अंकुश लगाने से दुःखदायी कुण्ठाओं का जन्म हो जाता है। प्रायः सभी धर्मां ने मनुष्य यंत्रणाओं का विशद चित्रण एवं वर्णन किया है जिससे मानव के हित की अपेक्षा अहित अधिक हुआ है।
काम एक ऊर्जा है तथा उसे विवेक द्वारा दिशा दिया जाना ही स्वस्थ हो सता है. यौन एक नैसर्गिक प्रवृत्ति है किन्तु इसे दोषमय एवं लज्जास्पद मानकर तथा पाप की संज्ञा देकर व्यक्तित्व के विकास पर घोस कुठाराघात किया जाता है। यह एकतथ्य है कि मनुष्य जितेन्द्रिय होकर ही जीवन में कुछ उपलब्धि कर सकता है किन्तु यौन को पापमय कहकर तथा मनुष्य को नरक आदि के दण्ड भोगने का भय दिखाकर उस पर बरबस अंकुश लगाना बौद्धिकता पर प्रहार करना तथा उसे कुण्ठित करना है। यौन जीवन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पक्ष है किन्तु समस्त चारित्रिक गुणों को केवल यौन-पक्ष में ही समेटकर तथा यौन-पक्ष को ही नैतिकता का एकमात्र आधार मानकर, किसी व्यक्ति को भला या बुरा घोषित कर देना अनुदारता है। यह एक तथ्य है कि अनेक तरुण और तरुणी मात्र दैहिक आकर्षण में फँसकर मनोपीडा के कारण यौन-हताश में भटक जाते हैं तथा बहुमूल्य जीवन को नष्ट कर देते है और अनेक नासमझ लोग वैवाहिक सूत्रों में बँधकर भी कहीं जाल मं फँसकर ग्लानिपूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जात हैं तथा कभी-कभी प्रेम-त्रिकोण के कारण निर्लज्ज अपराधी हो जाते हैं। मनुष्य को विवेक के जागरण द्वारा चिन्तन और आचरण को मर्यादित करना चाहिए।
अवैध यौनाचार का चस्का पड़ने पर पुरुष को अपनी पत्नी ही नहीं परिवार भी बादक प्रतीत होने लगता है तथा मनुष्य नए-नए जालों में स्वयं ही फँसने लगात है किन्तु विवेकशील पुरुष मर्यादा के अतिक्रमण को भटकना मानकर वासना-जाल से दूर ही रहता है। विवाह-पद्धति मानव-सभ्यता की एक उपलब्धि है तथा उसकी निर्धारित मर्यादा का पालन-व्यक्ति के विकास एवं समाज की व्यवस्था के हित में होता है किन्तु विवेकशील मनुष्य नियमों का पालन आत्मानुशासनकी दृष्टि से करता है, भयभीत होकर नहीं। वासनामय आकर्षण पतनकाल दोष होता है किन्तु गुणसम्मान होकर नही। वासनामय आकर्षण पतनकारक दोष होता है किन्तु गुणसम्मान के आधार पर मैत्रीपूर्ण निश्छल नाते कभी क्लेशप्रद नहीं होते।
मनुष्य से भूल होना स्वाभाविक है। संसार में किससे भूल नहीं होती ? कौन अन्तर्विरोधों, कुण्ठाओं और भयों से पूर्णतः मुक्त है? कौन पूर्ण है? अन्तर्विरोधों, कुण्ठाओं और भयों से पूर्णतः मुक्त है? कौन पूर्ण है? भूल को पाप मानकर मन को कुण्ठाग्रस्त करने से मनुष्य का आन्तरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विवेकशील व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर लेता है तथा भूल की पुनरावृत्ति न करने का प्रयत्न करता है। भूल को स्वीकार करने पर भी यदि भूल की पुनरावृत्ति होती है तो भी भूल को स्वीकार करने के कारण उसका वेग कम हो जाता है तथा धीरे-धीरे भूल समाप्त हो जाती है। विवेख द्वारा भूल के समाप्त होने से इच्छाशक्ति दृढ होती है तथा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब भूल चिन्तन को झकझोर देती है, वह विवेक की उत्प्रेरक तथा उपयोगी हो जाती है। यह भूल का उत्तम पक्ष है।
कभी-कभी हम अपने स्वाभाविक विचारों से ही चौंक जाते हैं। ये क्षणिक विचार अथवा कल्पना नितान्त सामान्य और स्वाभाविक होते हैं। किन्तु हम भय के कारण असामान्य मानकर उन्हें अनावश्यक महत्त्व दे देते हैं तथा भ्रान्त एवं चिन्तित हो जाते हैं। वास्तव में मन का स्वभाव कहीं-से-कहीं पहुँच जाना है तथा कल्पनाक्रम प्रारंभ होते ही मन वायु में उड़ते हुए पत्ते की भाँति आश्चर्यजनक स्थलों तक पहुँच जाता हैं जिसका उपयोग करने में कल्पनाशील लेखक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं किन्तु हम व्यर्थ ही उनेहं दोषपूर्ण मानकर भ्रान्त एवं भयभीत हो जाते हैं। हमं निराधार आशंकाओं को महत्त्व नहीं देना चाहिए। अविवेक के कारण मनुष्य राई को पहाड़ बना देता है। कभी-कभी कल्पना के पंख मनुष्य को विचार-श्रृंखला के प्रारम्भबिन्दु से इतनी दूर ले जाते हैं कि वह उसे भूल जाता है तथा स्वयं से पूछता है-मैं क्या करह रहा था? यह सब स्वाभाविक है। हमें उनके घबराना नहीं चाहिए और शान्त होकर विचारों के प्रवाह को देखना चाहिए। वास्तव में चेतन-स्तर पर हमारी बुद्धि सुधार की दृष्टि से जाग्रत् एवं सक्रिय रहती है। अनेक बार हम किसी व्यक्ति अथवा घटना के विष्य में पुरानी आदत के कारण ऐसी कल्पना कर लेते हैं जो हमारे वैचारिक-स्तर एवं नैतिक-स्तर के अनुरूप नहीं होती किन्तु अभद्र विचार चेतन-स्तर पर प्रोत्साहन न पाकर स्वयं ही क्षीण हो जाते हैं। वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति के मन में ईर्ष्या-द्वेष, वासना आदि अनेक प्रकार के विकार और अनेक प्रकार भय रहते हैं जिनको मनुष्य देखना भी नहीं चाहता। यदि मुख पर कोई कालिख लग गयी है तो दर्पण मे देखकर उसे मिटाना चाहिए। यह एक तथ्य है कि दोषों का उन्मूलन उन पर दृष्टि जमाए रखने से नहीं, बल्कि गुणों की अभिवृद्धि करने के स्वयं हो जाता है।
हमें अपने भीतर झाँककर मन के दर्पण को देखने का साहस करना चाहिए तथा विकारों को स्वाभिक मानकर समझदारी और धैर्य से उनका धीरे-धीरे शमन करने का यत्न करना चाहिए। सभी दोष मानवीय होते हैं तथा पूर्ण निर्दोषता मात्र एक आदर्श है। दोषों से निर्दोषता, अपूर्णता से पूर्णता की ओर बढते रहने में जीवन की सार्थकता है। मन मे सद्भाव आते ही हमें उनका सदुपयोग करना चाहिए तथा ईर्ष्या-द्वेष, भय आदि विकारों के साथ सीधे न लड़कर सद्भावों और सत्कर्मों द्वारा उन्हें क्षीण करना चाहिए। मानव सुलभ दोषों को देखकर चौंकने के बजाए धैर्यपूर्वक उनका, शोधन करना चाहिए। प्रश्न है कि मैंने कितना सीखा तथा मैंने कल की अपेक्षा आज कितना अधिक प्रयत्न किया। सच्चा पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं होता। गतिशील रहना, आगे बढ़ते रहना ही तो जीवन है। बस, चलते रहो, रुको मत। प्रयत्न करने में प्रसन्नता सन्निहित है। मुसाफिर के लिए हर कदम एक मंजिल है। जीवन की सार्थकता जीवन्तता बनाए रखने में है। जो ग्रन्थ, गुरु, दर्शन और उपदेश मनुष्य को भीतर उत्साह और आनन्द भरकर आगे बढने की प्रेरणा दे, वह सराहनीय है।
जीवन को एक मधुरसंगीत बनाने के लिए कुछ गुणों की प्रस्थापना तथा दोषों का निर्मूलन करना नितान्त आवश्यक है। यह कहना तर्क संगत नहीं है कि गुणों की प्रस्थापना से पूर्व दोषों को निर्मूल कर मन को रिक्त कर लेना चाहिए। वास्तव में चिन्तन, प्रेम और परमार्थ (परोपकार) इत्यदि गुणों की प्रस्थापना द्वारा समस्त दोषों का शमन स्वतः ही हो जाता है जैसे प्रकाश की किरणों से अन्धकार की शक्तियाँ स्वयं ध्वस्त हो जाती है। गुणों के विकास एवं दोषों के उन्मूलन की दोनों प्रक्रिया साथ ही चलती हैं। यद्यपि हमारे लिए अपने मानवीय दोषों को जान लेना और उन्हें पहचान लेना आवश्यक है, तथापि दोषों पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित करने से वे दृढ हो जाते हैं। वास्तव में चिन्तन, प्रेम, परमार्थ और पुरुषार्थ द्वारा जीवन-स्तर ही ऊँचा हो जाता है तथा सब दोषों का शमन स्वतः हो जाता है।
The Lodge Goat, Goat Rides, Butts and Goat Hairs, Gathered From the Lodge
Rooms of Every Fraternal Order (Pettibone)
-
The Lodge Goat, Goat Rides, Butts and Goat Hairs, Gathered From the Lodge
Rooms of Every Fraternal Order: More than a Thousand Anecdotes, Incidents
and Ill...
6 months ago
 My Channel
My Channel Cepek Arts
Cepek Arts Cepek Kids
Cepek Kids Cepek Media
Cepek Media Cepek Photography
Cepek Photography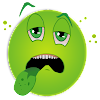 Social Fever
Social Fever
No comments:
Post a Comment