मनुष्य के चिन्तन के दो पक्ष होते हैं—विचारात्म्क् तथा भावात्मक। यद्यपि केवल मस्तिष्क ही विचार और भावनाओं का केन्द्र है, प्राय: भावना को ह्रदय से सम्बद्ध किया जाता है क्योंकि भावना का सीधा प्रभाव ह्रदय पर तत्काल होता है। वास्तव में भावना भी विचार का ही अंश होती है किन्तु वह उसकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होती है। भावना के कार्य के पृष्ठ में उसे करने का भावात्मक पक्ष सन्निहित होता है। भावना के बिना कर्म निष्प्राण एंव नीरस होता है। भावना का अतिरेक भावुकता का रुप लेकर मनुष्य को भटका देता है। भावना ही उद्वेग को जन्म देती है। मनुष्य भावना के सदोष हो जाने एंव भावुकता के प्रबल होने को अपने विवेक द्वारा नियंत्रित कर सकता है जो प्रकाश की भांति मनुष्य के जीवन-पथ को आलोकित कर देता है तथा उचित एंव अनुचित, न्याय एंव अन्याय, पुण्य एंव पाप और धर्म एंव अधर्म को स्पष्ट करके ठीक निर्णय लेने में सहायक होता है। विवेक को निरस्कार करेन पर मनुष्य चालाक लोगों की कठपुतली हो जाता है। विवेक का त्याग करने पर मनुष्य धर्मान्धता, अंधविश्वास, रुढिवादिता ओर कट्टरता के कुचक्र में फंसकर पशुवत् आचरण करने लगता है।
मनुष्य अपने किसी विचार से प्रेरित होकर ही उतम अथवा अधम चिन्तन तथा सत्कर्म करने में प्रवृत होता है। अतएव मनुष्य पर्याप्त सीमा तक अपने सारे सुख और दु:ख, उन्नति और अवनति, समद्धि और दरिद्रता तथा यश और अपयश के लिए स्वयं ही उतदरदायी होता है। सुख और दु:ख के कारण हमारे भीतर ही होते है। कभी हम क्रोध से उतेजित होकर, कटुता उत्पन्न करके व्यर्थ ही दूसरों को शत्रु बना लेते हैं, और फिर पछताते हैं, कभी हम भय और चिन्ता से ग्रस्त होकर पौरुषहीन एंव दयनीय बन जाते हैं, कभी विवेक खोकर अनुचित व्यवहार कर देते हैं और कभी शोकादि के आवेश में भावुकतावश अपने जीवन को एक बोझ बना लेते हैं, कभी सम्मान एंव सता की भूख और आलोचना से परेशान हो जाते हैं, कभी सहसा धनपति हो जाने की उत्कण्ठा से उद्विग्न हो जाते हैं तथा जीवन-यात्रा में संभलकर आगे बढ़ने के बजाए अकारणद ही संसार और भगवान् को दोष देने लगते हैं। अपने दु:ख और दोषों के लिए भाग्य को अथवा दूसरों को दोष देना मनुष्य को यथार्थ चिन्तन तथा संघर्ष से हटाकर निकम्मा बना देता है। मनुष्य चिन्तन द्वारा ही चिन्तन को स्वस्थ दिशा में मोड़ सकता है तथा ध्यान द्वारा शान्त और सबल और बना सकता है। मनुष्य का साधारण-सा प्रेरक विचार भी समग्र चेतना को प्रभावित कर देता है।
ध्यान से पूर्व तटस्थ चिन्तन करने के समय कुछ मिनिटों तक अपने विचार-जगत् को देखने और समझने के लिए धैर्य होना अत्यावश्यक हैं। तटस्थ चिन्तन का अर्थ है अपने ही विचारो भावनाओं, इच्छाओं, कल्पनाओं और उद्वेगों को एक दर्शक की भातिं उनमें लिप्त हुए बिना ही देखना। अनेक बार मनुष्य अपने ही पिचारों एंव भीषण कल्पनाओं से भयभीत हो जाता है तथा अपने मन को उनकी ओर से तत्कालल मोड़ लेना चाहता है। उसके चित में अपने विषय में अनेक प्रकार की आशांकाएं आने लगती हैं—क्यों मैं एक अभागा व्यक्ति हूं, क्या मेरी समस्याओं का कोई समाधान नहीं है, क्या मैं दोषो से भरा हुआ अधम पापी हूं, क्या मेरा भविष्य अन्धकारमय है, क्या मैं शोचनीय दिशा में जा रहा हूं, क्या मेरा अन्त खराब है। तटस्थ चिन्तन में क्लेशप्रद एंव उतेजनाप्रद विचारों की ओर उपेक्षाभाव रखने से वे ऐसे ही चले जायेंगे जैसे स्वागत न होने पर बिना बुनाए हुए अभद्र अतिथि, किन्तु रुचिकर पूर्वक ध्यान देने से वे सबल करने से भयप्रद आंशका तथा विचार क्षीण होकर निष्प्रभाव हो जाएंगे।
इसके अतिरिक्त भी हमें कभी-कभी एकान्त में बैठकर विवेपूर्वक आत्मवलोकन करना चाहिए अर्थात् अपने विचारों और आचरण का धैर्यपूर्वक निरीक्षण करना चाहिए कि क्या ग्रह्यय ओर क्या त्याज्य है। वास्तव के संसार के प्रत्येक मनुष्य में कुछ दुर्बलता और दोष होते हैं तथा प्रत्येक मनुष्य में संकल्प-शक्ति एंव प्रयत्न द्वारा उनसे ऊपर उठने की अर्थात उनसे मुक्त होने की क्षमता अवश्य होती है।
The Lodge Goat, Goat Rides, Butts and Goat Hairs, Gathered From the Lodge
Rooms of Every Fraternal Order (Pettibone)
-
The Lodge Goat, Goat Rides, Butts and Goat Hairs, Gathered From the Lodge
Rooms of Every Fraternal Order: More than a Thousand Anecdotes, Incidents
and Ill...
3 months ago
 My Channel
My Channel Cepek Arts
Cepek Arts Cepek Kids
Cepek Kids Cepek Media
Cepek Media Cepek Photography
Cepek Photography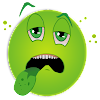 Social Fever
Social Fever
No comments:
Post a Comment